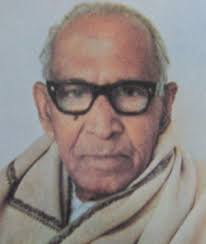
सन् 1926-27 में डॉ. मोहनसिंह मेहता को यूरोप में अपनी एक यात्रा के दौरान एक ट्रेन के लिए एक घण्टे से अधिक के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रतीक्षालय में बैठे हुए उन्होंने अपनी डायरी में एक प्रगतिशील विद्यालय (प्रोग्रेसिव स्कूल) की योजना के बारे में लिखा, ऐसा विद्यालय जो बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास हेतु लाॅर्ड बैड़न पावेल के ‘‘बायज स्काउट मूवमेण्ट’’ की पद्धति पर आधारित हो।

दूसरी बार फिर वही सपना डाॅ. मोहनसिंह मेहता के चेतन मन में उभरा, मई 1930 में जब वे स्काउटिंग ट्रूप के लिए कश्मीर गए। एक बारिश के दिन गुलमर्ग में शैक्षिक चर्चा के दरमियान उन्होंने नए प्रकार के विद्यालय के विचार को विकसित किया।
16 जनवरी, 1931 को विद्याभवन स्कूल की इमारत की आधार शिला मेवाड़ राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री सुखदेव प्रसाद द्वारा रखी गई। विद्याभवन स्कूल 21 जुलाई, 1931 को देवगढ़ की हवेली में प्रारम्भ किया। सिर्फ चार कक्षाओं (पांचवी से आठवीं तक) 58 विद्यार्थियों और 10 अध्यापकों से इस विद्यालय का आरम्भ हुआ। इस संस्थान के प्रथम प्रधानाध्यापक डॉ. कालूलाल श्रीमाली थे। जो बाद में इसी संस्थान में अध्यापक शिक्षा संस्थान 1942 के प्राचार्य रहे और भारत के केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, बनारस एवं मैसूर विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर रहे। इस तरह डॉ. मोहनसिंह मेहता का एक प्रायोगिक, प्रगतिशील, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना का स्वप्न साकार हुआ।
वस्तुतः विद्याभवन जैसी प्रगतिशील एवं नवाचार आधारित संस्था को आरम्भ करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य था शिक्षा के माध्यम से समाज का पुनर्निर्माण। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उसके सर्वांगीण विकास हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। बच्चों में व्यापक दृष्टिकोण व अपने वातावरण के अनुकूल समायोजन की क्षमता पैदा करना, ऐसे उपयोगी नागरिक तैयार करना जिन्हें समाज के प्रति अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का बोध हो। विद्यार्थियों के इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना।
आम परम्परावादी विद्यालयों से हटकर एक ऐसे विद्यालय का सपना डॉ. मेहता ने देखा, जिसमें शिक्षा-बाल केन्द्रित हो और मनोविज्ञान पर आधारित हो। बच्चे को स्वतंत्र वातावरण मिले अधिगम स्थितियां आनंददायक हों, खेल का पर्याप्त अवसर मिले। वह श्रम तथा हस्तकार्य कर सके, सृजनात्मकता तथा सामाजिक गुणों का विकास हो सके। कल्पना शक्ति तथा अभिव्यक्ति के विकास हेतु पर्याप्त अवसर मिले। कुल मिलाकर ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना जिससे प्रत्येक बच्चे का उसकी क्षमतानुसार पूर्ण विकास हो सकें।
उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिन आधारभूत तत्वों को अपनाया गया वे जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय के आधार पर भेदभाव से रहित वातावरण तैयार करना। संकीर्णताओं से हटकर सभी विद्यार्थी साथ-साथ बैठकर भोजन करते थे। विद्यालय में सफाई करने वाले कर्मचारी (भंग) का बच्चा भी शाम को दूसरे बच्चों के साथ खेलता था। इस प्रकार के माहौल में पल बढ़कर यहां के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में व्यापकता एवं विशालता जीवन शैली का एक अंग बन जाती।
प्राथमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर सहशिक्षा भारत में कई स्थानों पर प्रचलित थी, किन्तु माध्यमिक स्तर पर यह असामान्य बात थी। विद्यालय में सहशिक्षा का आरम्भ राजस्थान के तत्कालीन माहौल में वास्तव में एक मौलिक एवं साहसिक कदम था। विद्याभवन में अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास की दृष्टि से दूसरे देशों से उपयुक्त व्यक्तियों को जिनका विद्याभवन के सामाजिक एवं शैक्षिक उद्देश्यों में विश्वास हो, काम करने के लिए बुलाया गया।
विद्यालय के प्रति सख्त दृष्टिकोण की इस समय की आम धारणा के विपरीत प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व को महूत्व दिया गया। प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं विद्यार्थियों के बीच सम्बन्ध आत्मीय एवं निकटता के हों जिससे अनुशासन ऊपर से थोपा हुआ न होकर स्वतः पैदा हो, यह प्रयास किया गया।
उद्देश्यों के अनुरूप विद्यार्थियों को तैयार करने में बाह्य तत्व प्रभावी न हो इस दृष्टि से विद्याभवन को पूर्ण दिवसीय (प्रातरू से संध्या तक) विद्यालय बनाने का निश्चय किया गया। छात्रावास की सुविधा आंशिक रूप से विद्यालय में उपलब्ध थी, किन्तु पूरे दिन के स्कूल से सभी विद्यार्थियों को आवासीय विद्यालय जैसा लाभ मिल सका।
विद्याभवन की विशिष्टताओं में दल पद्धति प्रमुख है, जिसके अन्तर्गत बच्चों को अलग-अलग दलों में बांट दिया जाता है। लगभग दो अध्यापक एक दल के प्रभारी होते हैं। बच्चों की प्रगति का पूरा रिकाॅर्ड रखना, उनके अभिभावकों से समय-समय पर सम्पर्क करना, हाईक व रात्रि कैम्प का आयोजन करना तथा अन्य पाठ्य सहगामी प्रवृतियों का आयोजन करना, जिससे छोटे समूह में हरेक बच्चे पर ध्यान दिया जा सके और उसकी अन्तर्निहित शक्तियों व रुचियों को पहचान कर उसके चहुमुखी विकास हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान किया जा सके। दल में विद्यार्थी अपनी समस्याओं, कठिनाइयों व जिज्ञासाओं के बारे में खुलकर बातचीत कर सकते हैं और अध्यापक प्रत्येक बच्चे को अच्छी तरह समझकर समय-समय पर उन्हें उचित मार्गदर्शन देते हैं।
वनशाला विद्याभवन का एक सर्वथा अनूठा एवं अनुभवसिद्ध सफल प्रयोग है। नियमित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों से हटकर अध्ययन, चिंतन-मनन, अवलोकन, अभिव्यक्ति एवं भ्रमण वनशाला के प्रमुख अंग हैं। वनशाला एक साधारण कैम्प नहीं वरन् प्रकृति के उन्मुक्त एवं रमणीक वातावरण में एक अभूत विद्यालय है। शाला की प्रवृतियां कहीं वन में हों, यही वनशाला है।
वनशाला के लिए निर्धारित स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए इतिहास, भूगोल, साहित्य, संगीत, कला, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन आदि श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। विद्यालय से दूर किसी निर्जन स्थल में 10-15 दिन अपने परिवार जन से अलग रहकर विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, श्रम के प्रति निष्ठा, पारस्परिक सहयोग, पर्यवेक्षण कुशलता एवं नेतृत्व के गुणों का विकास होता है।
वार्षिकोत्सव प्रायोजना के अन्तर्गत इस विषय (थीम) का चयन करके, विद्यार्थियों को उनकी रूचि अनुसार निर्धारित विषय के विभिन्न पक्षों पर आधारित अध्ययन के लिए अलग-अलग समूहों में बांट दिया जाता है। प्रायोजना कार्य के अन्तर्गत विषय से सम्बन्धित वार्ताओं का आयोजन - फिल्म शो, लेख, नक्शे, चाटर््स, माॅडल, चित्र आदि तैयार किए जाते हैं, जिनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। वार्षिकोत्सव का दूसरा पक्ष ‘‘पैजेण्ट’’ के रूप में सामने आता है, जिसमें चयनित विषय से सम्बन्धित नाटक, झांकियां, छाया दृश्य, गीत, नृत्य आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार वार्षिकोत्सव में विद्यार्थी देखकर, सुनकर और स्वयं करके बहुत सीख लेते हैं।