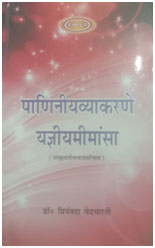
हमारे गुरुकुलों में बालक बालिकाओं को प्राचीन आर्ष संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी-महाभाष्य पद्धति का ऋषि दयानन्द निर्दिष्ट पद्धति से अध्ययन कराया जाता है। अध्ययन करने के बाद कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी शोध उपाधि पी.एच-डी. प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। उनका प्रिय विषय वेद, दर्शन, उपनिषद, वैदिक साहित्य सहित व्याकरण आदि हुआ करते हैं। आर्यसमाज में अनेक छात्रों व विद्वानों ने संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर वैदिक विषयों में पी.एच-डी. किया है जिनमें से कुछ विद्वानों के चर्चित शोध प्रबन्ध प्रकाशित भी हुए हैं। इसी परम्परा में प्रस्तुत ग्रन्थ ‘पाणिनीयव्याकरण में यज्ञीयमीमांसा’ एक है। इस ग्रन्थ का प्रणयन वेद विदुषी आचार्या डा. प्रियंवदा वेदभारती जी, व्याकरणाचार्या, वेदनैरुक्ताचार्या, प्राचार्या, गुरुकुल-कन्या आर्ष विद्यापीठम् (श्रवणपुरम्) नजीबाबाद-246763 (उत्तरप्रदेश राज्य) ने किया है। इस ग्रन्थ के महत्व को जानकर आर्य साहित्य के एक प्रमुख प्रकाशक श्री प्रभाकरदेव आर्य, हिण्डोनसिटी ने इसका प्रकाशन अपने प्रकाशन संस्थान हितकारी प्रकाशन समिति, हिण्डौन सिटी-322230 की ओर से किया है। पुस्तक प्राप्त करने के लिए प्रकाशक श्री प्रभाकरदेव आर्य जी से उनके मोबाइल नम्बर 7014248035 एवं 9414034072 पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह ग्रन्थ संस्कृत व हिन्दी दोनों भाषाओं में एक ही जिल्द में प्रकाशित किया गया है। पुस्तक के आरम्भ में संस्कृत भाग तथा उसके बाद हिन्दी भाग दिया गया है। पूरा ग्रन्थ 652 पृष्ठों का है जिसमें संस्कृत भाग 314 पृष्ठों का तथा शेष भाग हिन्दी में है। पुस्तक श्री ऋषिदेव जी, बी-221, नेहरू विहार दिल्ली-110054, www.vedrishi.com, चलभाष 9818704609 सहित डा. प्रियंवदा वेदभारती जी एवं श्री गणेशदास-गरिमा गोयल, वैदिक साहित्य प्रतिष्ठान, 4058-59, बिजली घर के सामने, नया बाजार, दिल्ली-110006 से प्राप्त की जा सकती है। पुस्तक सन् 2018 में राधा प्रेस, साहिबाबाद (उत्तरप्रदेश) से मुद्रित होकर प्रकाशित हुई है। लेखिका महोदया ने अपनी इस पुस्तक ऋषिभक्त एवं आर्ष व्याकरण के उच्च कोटि के विद्वान आचार्य विजयपाल जी, रामलाल कपूर न्यास को समर्पित की है।
किसी भी पुस्तक का परिचय सार रूप में उसकी प्रस्तावना वा भूमिका में दिया जाता है। अतः हम प्रस्तावना का कुछ भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। लेखिका प्रस्तावना में लिखती हैं कि यद्यपि व्याकरण का क्षेत्र प्रकृति-प्रत्यय के संश्लेषण-विश्लेषण द्वारा शब्दों का साधुत्वान्वाख्यान ही है तथा ‘सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे’ शब्दों के साथ अर्थ और सम्बन्ध की नित्यता होने से शब्दसाधुत्व प्रतिपादक पाणिनीय व्याकरण वांग्मय के उदाहरणों, प्रत्युदाहरणों, वात्र्तिकों तथा वात्र्तिक व्याख्याओं में पाणिनि-कात्यायन-पतंजलि कालीन समस्त बृहत्तर भारत प्रतिबिम्बित होता है, यह भी सत्य है। लेखिका आगे लिखती हैं कि इस मुनि त्रयी के वांग्मय का अध्ययन करने से यह सुतरां स्पष्ट है कि इनके काल में याज्ञिक ग्रन्थों का और यज्ञ प्रक्रियाओं का बहुत विस्तार और प्रचार था, अग्निष्टोम आदि सोमयागों तथा दर्शपौर्णमासादि हविर्यागों का वर्णन न केवल श्रौतसूत्रों में था प्रत्युत इन सभी यागों के पृथक्-पृथक् व्याख्यान ग्रन्थ भी थे। ये ग्रन्थ आग्निष्टोमिक, राजसूयिक, वाजपेयिक, ऐष्टिक, पाशुक आदि नामों से विख्यात थे। विशिष्ट यागों के अतिरिक्त इनके अंगभूत पुरोडाश, चतुर्होतारः, पंचहोतारः आदि के लिये भी पृथक् व्याख्यानग्रन्थ थे, यह पौरोडाशिकः, पुरोडाशिकः, चातुर्होतृकः, पांचहोतृकः आदि उदाहरणों से ज्ञात होता है। याज्ञिक क्रियाओं-उपक्रियाओं से अभिव्याप्त काल में रचे गये व्याकरण ग्रन्थों में यज्ञ की चर्चा न हो यह कैसे सम्भव है? महाभाष्यकार पंतजलि ‘वेदः-खल्वपि’ कहकर जो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं वे सब प्रायः यज्ञविषयक ही होते हैं। उन्होंने व्याकरण के अट्ठारह प्रयोजनों में से सात प्रयोजन यज्ञ से सम्बन्धित ही रखे हैं। इससे स्पष्ट है कि जैसे लोक में व्याकरण के बिना कार्य नहीं चल सकता वैसे ही यज्ञों में भी याज्ञिकों का कार्य व्याकरण के बिना नहीं चल सकता। स्वर-वर्ण-त्रुटिराहित्य के लिये व्याकरण का आश्रयण अनिवार्य है। प्रस्तावना में इनके बाद व्याकरणग्रन्थों में निहित कर्मकाण्डगत सूक्ष्म भेद पर प्रकाश डालने के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रवृत्तिनिमित्त सूचित करते हुए जो विद्वान आदि इस ग्रन्थ के शोध व लेखन में सहयोगी रहे हैं उनका आभार प्रदर्शन किया है।
प्रस्तावना के बाद पुस्तक की विस्तृत विषयानुक्रमणिका दी गई है। पुस्तक में आठ मुख्य अध्याय एवं तीन परिशिष्ट हैं। इनका संक्षिप्त उल्लेख भी पाठकों के लिए कर रहे हैं जो कि निम्न हैः-
प्रथम अध्यायः पाणिनीय वांग्मय का परिचय, पृष्ठ 327-354
द्वितीय अध्यायः याज्ञ वांग्मय का परिचय, पृष्ठ 355-401
तृतीय अध्यायः यज्ञयज्ञीयदक्षिणाविवेचन, पृष्ठ 402-446
चतुर्थ अध्याय: ऋत्विग् यजमानविषयक विवेचन, पृष्ठ 447-500
पंचम अध्याय: देवता विवेचन, पृष्ठ 501-521
षष्ठ अध्याय: यज्ञीय सम्भार विवेचन, पृष्ठ 522-582
सप्तम अध्याय: इतिकर्तव्यतागत-वाक्य-निगद स्तोमादि विवेचन, पृष्ठ 583-617
अष्ठम अध्याय: विप्रकीर्णविषयक, पृष्ठ 618-628
परिशिष्ट-1 यज्ञों का प्रवृत्तिनिमित्त और पशुयाग (श्री पं. युधिष्ठिर मीमांसक जी की दृष्टि में)
परिशिष्ट-2 पशुयाग (आचार्य उदयवीर शास्त्री जी की दृष्टि में)
परिशिष्ट-3 पणिनीय व्याकरण में यज्ञों से सम्बन्धित गणितीय प्रयोग (डा. सुद्युम्नाचार्य)
सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची: पृष्ठ 647-652
पुस्तक के अन्तिम कवर पृष्ठ के भीतर की ओर अंग्रेजी पुस्तक ‘फाउण्डर्स आव् साइन्सेज इन एन्शेण्ट इण्डिया’ का हिन्दी अनुवाद ‘प्राचीन भारत के वैज्ञानिक कर्णधार’ के प्राक्कथन के स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जी लिखित कुछ भाग को उद्धृत किया गया है। इस महत्वपूर्ण अंश को भी हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वामी (डा.) सत्यप्रकाश सरस्वती जी ने लिखा है ‘‘वैदिक संहिताओं में मन्त्रों के प्रारम्भ में परम्परा से जिन ऋषियों की सूची हमें प्राप्त है, हम यह तो नहीं स्वीकार करते कि ऋचायें उनकी कृति थीं-किन्तु उन ऋचाओं के मर्म और रहस्यों का उन ऋषियों ने सर्वप्रथम उद्घाटन किया था। कुछ ऋचाओं का ऋषि अंगिरा है, अथर्वण है, इस अथर्वण और उसके सहयोगियों ने अग्नि का सर्वप्रथम मन्थन किया, और यज्ञों की परम्परा डाली। अग्नि के उपयोग के साथ-साथ अनेक आविष्कारों और अनुसन्धानों का प्रारम्भ हुआ। भारत में (केवल भारत में ही प्राचुर्य से और ईरान में भी कुछ-कुछ) इन्हीं यज्ञस्थलियों में बैठकर प्राचीन मनीषियों ने अनेक विज्ञानों की नींव डाली। यज्ञ में प्रयुक्त यज्ञशाला के उपकरण स्वयं में अनोखे आविष्कार हैं, जिन्होंने यांत्रिकी की आधारशिला रखी। ये यज्ञस्थलियां हमारी प्राथमिक कार्यशालायें, अनुसंधान शालायें और वेधशालायें बनी, जिनके माध्यम से ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हमने उत्तरोत्तर प्रगति की। यज्ञों के लिए जो पात्र विभिन्न क्रियाओं के निमित्त बने, वे ही हमारी आयुर्वेदशालाओं के उपकरणों में परिवर्तित हो गए, और ये गृहस्थलियों की पाकशाला के भी संभार और पात्र बने। विविध चक्र-चरखा-करधा, रथचक्र, कौलालचक्र, सुदर्शनचक्र इनकी नींव भी वैदिक युग में पड़ी। लम्बाई, चौड़ाई, तौल और काल की मापों का हमने प्रयोग सीखा। क्षुरा, चाकू, सूत और डोरी, और सुश्रुत काल के शल्य-यन्त्र, कोल्हू, किसानी के हल, और खोदाई के उपकरण और उनके साथ-साथ खनिजों, धातुओं और मृदाओं का प्रयोग हमने सीखा। वनस्पतियों और ओषधियों से हमारा परिचय बढ़ा।”
पुस्तक के अन्तिम कवर पृष्ठ पर पुस्तक की लेखिका आचार्या डा0 प्रियंवदा वेदभारती जी का केवल संस्कृत में परिचय दिया गया है। यह लेखिका-परिचय प्रो0 महावीर अग्रवाल, व्याकरणाचार्य, एम.ए. (वेद, संस्कृत और हिन्दी), डी.लिट्. पूर्व अध्यक्ष-संस्कृत विभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार तथा पूर्वकुलपति उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार ने लिखा है।
हमारे जो विद्वान शोध प्रबन्ध लिखते हैं उसमें वह उस विषय का तलस्पर्शी व गहन अध्ययन कर विषय के सभी पक्षों पर तर्क युक्त विचार व समीक्षायें प्रस्तुत करते हैं। यह शोधकर्ताओं की अनेक वर्षों की तपस्या व परिश्रम होता है जिसे हम कुछ ही दिनों में पढ़कर लाभान्वित होते हैं। शोधप्रबन्ध पढ़कर पाठक को शोधलेखक के समान विषय का उच्चस्तरीय ज्ञान हो जाता है। अतः हमें शीर्ष विद्वानों के ग्रन्थों के साथ शोध प्रबन्धों को पढ़ने का अभ्यास भी करना चाहिये। ऐसा करने से हमें उस शोध विषय का समुचित ज्ञान हो सकता है। लेखिका महोदया अपने शोध कार्य को प्रकाशक श्री प्रभाकरदेव आर्य जी की सहायता से विद्वतवर्ग तक पहुंचाने में जो सत्प्रयास किया है इसके लिए हम इस पुस्तक का अभिनन्दन करते हैं और गुरुकुल के उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों व स्नातकों को इस पुस्तक को प्राप्त कर इसका अध्ययन करने का निवेदन करते हैं। ऐसा करने से शोधकत्र्री आचार्या डा. प्रियंवदा वेदभारती जी सहित प्रकाशक महोदय का परिश्रम सफल होगा। ओ३म् शम्।
-मनमोहन कुमार आर्य
पताः 196 चुक्खूवाला-2
देहरादून-248001
फोनः09412985121