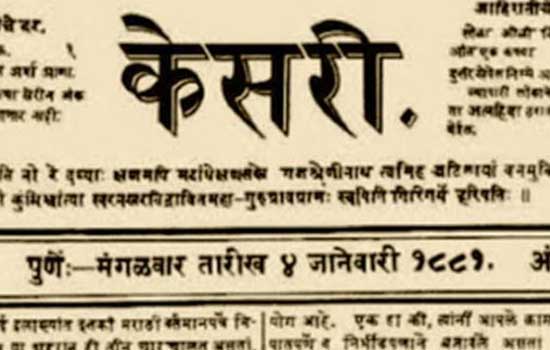
कोटा | भारत में समाचार पत्रों का उदभव ऐसे समय हुआ जब न तो स्वतंत्रता की अभी व्यक्ति थी, न आज जैसे संसाधन थे ऊपर से थे अनेक प्रतिबंध।समाचार पत्र (Newspaper)निकलना टेढ़ी खीर था। जरा सा भी सत्ता के विरोध में लिखा या तो समाचार पत्र बंद कर दिया जाता था या छापाखाना ही जप्त कर लिया जाता था। समाचार पत्र छापने वालों को को गिफ्तार तक कर लिया जाता था। ऐसे कई दमनकारी नियमों के बीच पत्र निकलना एक जनून से कम नहीं था। दमनकारी नियम पत्रकारिता की भड़की चिंगारी को बुझा न सके। पत्रकारों एवं समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिस अक्षर युद्ध की शुरुवात की वह बढ़ता गया और हमारे देशवासियों में आजादी की लो जलाने में मील का पत्थर बने। आइये ! जानते हैं अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने और दमनकारी नीतियों के चलते समाचार पत्रों के उद्भव की दास्तान।
भारत में समाचार पत्रों का इतिहास यूरोपीय लोगो के भारत में प्रवेश के साथ ही प्रारंभ होता हैं। सर्वप्रथम भारत में प्रिटिंग प्रेस (Printing press) लाने का श्रेय पुर्तगालियों का दिया जाता हैं। वर्ष 1557 ई में गोवा के कुछ पादरी लोगो ने भारत की पहली पुस्तंक छापी गई।वर्ष 1648 ई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी (British East India Company)ने भी भारत की पहली पुस्तक की छपाई की थी। कम्पनी ने ही 1684 ई में ही भारत में प्रथम प्रिटिंग प्रेस मुद्रणालय की स्थापना की थी।
भारत में पहला समाचार पत्र कम्पनी के एक असन्तुष्ट सेवक विलियम वोल्ट्स ने 1766 ई में निकालने का प्रयास किया लेकिन अपने इस कार्य में वह असफल रहा। इसके बाद भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय ‘‘ जेम्स आगस्टस हिक्की‘‘(James Augustus Hickey) को मिला। उसने 1780 ई में ‘बंगाल गजट‘ का प्रकाशन किया गया। किन्तु इससे कम्पनी सरकार की आलोचना की गई थी। जिस कारण उसका प्रेस जब्त कर लिया गया । इस दौरान कुछ अन्य अग्रेजी अखबारों बंगाल में ‘कलकता कैरियर‘ , ‘एशियाटिक मिरर‘, ‘ओरियटल स्टार‘ मद्रास में ‘मद्रास केरियर‘, मद्रास गजट, बम्बई में हेराल्ड , बाबे गजट आदि का प्रकाशन हुआ। बर्किघम ने कलकत्ता जनरल का सम्पादन किया। बर्किघम ही वह पहला प्रकाशक था जिसने प्रेस को जनता के प्रतिबिम्ब के स्वरूप में प्रस्तुत किया । प्रेस का आधुनिक रूप जेम्स सिल्क बर्किघम का ही दिया हुआ हैं। हिक्की तथा बर्किघम का पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान हैं । इन दोनों ने तटस्थ पत्रकारिता एवं स्वतंत्र लेखन का उदारहण प्रस्तुत कर पत्रकारों को पत्रकारिता की ओर आकर्षित किया ।
पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 ई में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा ‘बंगाल गजट‘ नाम से निकाला गया। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। मार्शमैन (Marshman) के नेतृत्व में 1818 ई. में बंगाली भाषा में ‘‘दिग्दर्शन‘‘ मासिक पत्र प्रकाशित हुआ लेकिन यह पत्र अल्पकालिक सिद्ध हुआ । इसी समय मार्शमैन के संपादन में एक और साप्ताहिक समाचार पत्र ‘‘ समाचार दर्पण‘‘ (News mirror)प्रकाशित किया गया। बंगाली भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र ‘संवाद कौमुदी‘ का प्रकाशन 1821 ई.में हुआ। इस समाचार पत्र का प्रबन्ध राजा राममोहन राय के हाथों में था। राजा राममोहन राय ने सामाजिक तथा धार्मिक विचारों के विरोधस्वरूप ‘‘समाचार चंद्रिका‘‘ का मार्च 1822 ई में प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त राय ने अप्रेल 1822 में फारसी भाषा में ‘‘मिरातुल‘‘ (Miratul) अखबार एवं अंग्रेजी भाषा में " ब्राहानिकल मैगजीन " (Brahmanical magazine) का प्रकाशन किया । वर्ष 1830 ई में राजा राममोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से बंगाली भाषा में बंगदूत ‘ का प्रकाशन आरंभ हुआ। मुम्बई से 1831 ई में गुजराती भाषा में "जामे जमशेद "तथा 1851 ई में ‘रास्त गोफ्तार" एवं "अखबारे सौदागार "का प्रकाशन हुआ।
समाचार पत्र पर लगने वाले प्रतिबंध के अन्तर्गत 1799 ई में लार्ड वेलेजली द्वारा पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम और जाॅन एडमस द्वारा 1823 में अनुज्ञप्ति नियम लागू किये गये । एडमस द्वारा समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध के कारण राजा राममोहन राय का मिरातुल अखबार बंद हो गया। लाॅर्ड विलियम बैटिंग (Lord William Batting) प्रथम गवर्नर -जनरल था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया । कार्यवाहक गर्वनर जनरल चार्ल्स मेटकाॅफ ने 1823 ई में के प्रतिबंध को हटाकर समाचार पत्रों को मुक्ति दिलाई । यही कारण हैं कि उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता हैं। लार्ड मैकाले (Lord Macaulay) ने भी प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। 1857-1858 के विद्रोह के बाद भारत में समाचार पत्रों को भाषाई आधार के बजाय प्रजातीय आधार पर विभाजित किया गया हैं। अंग्रेजी समाचार पत्रों एवं भारतीय समाचार पत्रों के दृष्टिकोण में अंतर होता था। जहां अग्रेजी समाचार पत्रों को भारतीय समाचार पत्रों की अपेक्षा ढेर सारी सुविधाऐं उपलब्ध थी वही भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा था। सभी समाचार पत्रों में ‘‘इग्लिश मैन‘‘ (English man) सर्वाधिक रूढिवादी एवं प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र था। ‘‘पायनियर‘‘ सरकार का पूर्ण समर्थक समाचार पत्र था, जबकि स्टेटमेंन कुछ तटस्थ दृष्टिकोण रखता था।
वर्ष 1857 ई में हुए विद्रोह के परिणामस्वरूप सरकार ने 1857 ई का ‘लाईसेंसिंग एक्ट ‘ लागू कर दिया । इस एक्ट के आधार पर बिना सरकारी लाईसेंस के छापाखाना स्थापित करने एवं उसके प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई । यह रोक एक वर्ष तक लागू रही । वर्ष 1867 ई के पंजीकरण अधिनियम का उद्देश्य छापाखानों को नियमित करना था। अब हर मुद्रित पुस्तक एवं समाचार पत्र के लिए यह आवश्यक कर दिया कि वे उस पर मुद्रक, प्रकाशक एवं मुद्रण स्थान का नाम लिखा जाये । पुस्तक के छपने के बाद एक प्रति निःशुल्क स्थानीय सरकार को देनी होती थी। वहाबी विद्रोह से जुडे लोगों द्वारा सरकार विरोधी लेख लिखने के कारण सरकार ने ‘‘भारतीय दण्ड संहिता‘‘ की धारा 124 में 124 क जोड कर ऐसे लोगों के लिए आजीवन निर्वासन , अल्प निर्वासन व जुर्माने के प्रावधान किये।
देेेश में 1857 ई. के संग्राम के बाद भारतीय समाचार पत्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और अब वे अधिक मुखर होकर सरकार के आलोचक बन गये । इसी समय बडे भयानक अकाल से लगभग 60 लाख लोग काल के ग्रास बन गये थे वही दूसरी ओर जनवरी 1877 में दिल्ली में हुए ‘‘दिल्ली दरबार‘‘ पर अंग्रेज सरकार ने बहुत ज्यादा फिजूलखर्ची की । परिणामस्वरूप लार्ड लिटन की साम्राज्यवादी प्रवृति के खिलाफ भारतीय अखबारों ने आग उगलना शुरू कर दिया समाचार पत्र अधिनियम द्वारा भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता नष्ट कर दी ।
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तत्कालीन लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र ‘‘ सोम प्रकाश ‘‘ को लक्ष्य बनाकर लाया गया था। दूसरों शब्दों में यह अधिनियम मात्र ‘सोम प्रकाश‘ पर लागू हो सका । लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ‘‘अमृत बाजार पत्रिका‘‘ (समाचार पत्र) जो बंगला भाषा की थी, अग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गयी । सोम प्रकाश , भारत मिहिर, ढाका प्रकाश सहचर आदि के खिलाफ मुकदमें चलाये गये। इस अधिनियम के तहत समाचार पत्रों को न्यायलय में अपील का कोई अधिकार नहीं था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को मुह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया हैं। आगे चल कर इस समाचार पत्र विरिधि अधिनियम को लार्ड रिपन ने 1882 ई में रद्द कर दिया ।
लार्ड कर्जन (Lord Curzon) द्वारा बंगाल विभाजन के कारण देश में उत्पन्न अशान्ति तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चरामपंथियों के बढते प्रभाव के कारण अखबारों के द्वारा सरकार की आलोचना का अनुपात बढने से समाचार पत्र अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि जिस अखबार के लेख में हिंसा व हत्या को प्रेरणा मिलेगी, उसके छापाखाने व सम्पति को जब्त कर लिया जायेगा। अधिनियम में किये गए प्रावधनों के अन्तर्गत 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की सुविधा दी गई । इस अधिनियम द्वारा नौ समाचार पत्रों के विरूद्ध मुकदमें चलाये गये एवं सात के मुद्रणालय को जब्त करने का आदेश दिया गया।
वर्ष 1910 ई के ‘‘ भारतीय समाचार पत्र अधिनियम" में यह व्यवस्था थी कि समाचार पत्र के प्रकाशक को कम से कम 500 रूपये और अधिक से अधिक 2000 रूपये पंजीकरण जमानत के रूप में स्थानीय सरकार को देना होगा, इसके बाद भी सरकार को पंजीकरण समाप्त करने एवं जमानत जब्त करने का अधिकार होगा । दोबारा पंजीकरण के लिए सरकार को 1000 रूपये या 10000 रूपये तक की जमानत लेने का अधिकार होगा। इसके बाद भी यदि समाचार की नजर में किसी आपतिजनक सामग्री को प्रकाशित करता है तो सरकार के पास उसके पंजीकरण को समाप्त करने एवं अखबार की समस्त प्रतियां जब्त करने का अधिकार होगा। अधिनियम के शिकार समाचार पत्र दो महीने के अन्दर स्पेशल टिब्यूनल के पास अपील कर सकते थे।
प्रथम विश्वयुद्ध के समय ‘‘ भारत सुरक्षा‘‘ अधिनियम पास कर राजनीतिक आन्दोलन एवं स्वतंत्रा आलोचना पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 1921 ई. में सर तेज बहादुर सपू्र की अध्यक्षता में एक ‘‘प्रेस इन्क्वायरी कमेटी‘‘ (Press inquiry committee)नियुक्ति की गई। समिति के ही सुझावों पर 1908 और 1910 ई. के अधिनियमों को समाप्त किया गया। वर्ष1931 ई में इंडियन प्रेस इमरजेन्सी एक्ट लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा 1910 ई के प्रेस अधिनियम को पुनः लागू किया गया। इस समय गांधी जी द्वारा चलाये गये सविनय अवज्ञा‘‘ आन्दोलन के प्रचार को दबाने के लिए इस अधिनियम को विस्तृत कर क्रिमिनल अमैडमेंट एक्ट अथवा आपराधिक संशोधित अधिनियम लागू किया गया। मार्च 1947 में भारत सरकार ने प्रेस इन्क्वायरी कमेटी की स्थापना समाचार पत्रों से जुडे हुए कानून की समीक्षा के लिए किया गया।
भारत में समाचार पत्रों एवं प्रेस के इतिहास के इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता हैं जहां एक ओर लार्ड वेलेजली , लार्ड मिण्टो, लार्ड एडमस, लार्ड कैनिंग तथा लार्ड लिटन जैसे प्रशासकों ने प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किया, वही दूसरी ओर लार्ड बैंटिक , लार्ड हेस्टिंग्स , चार्ल्स मेटकाफ , लार्ड मैकाले , एवं लार्ड स्पिन जैसे लोगो ने प्रेस की आजादी का समर्थन भी किया । अंग्रेजों के समाचार पत्र विरोधी रवैये एवं प्रतिबंधों के बावजूद भी तत्कालीन जांबाज पत्रकारों ने उनके जुल्म सह कर भी समाचार पत्रों का प्रकाशन कर पत्रकारिता की चिंगारी को बुझने नहीं दिया।