पुस्तक समीक्षा मंदिर संस्कृति - धार्मिक पर्यटन
समीक्षक डॉ. वैदेही गौतम साहित्यकार, कोटा
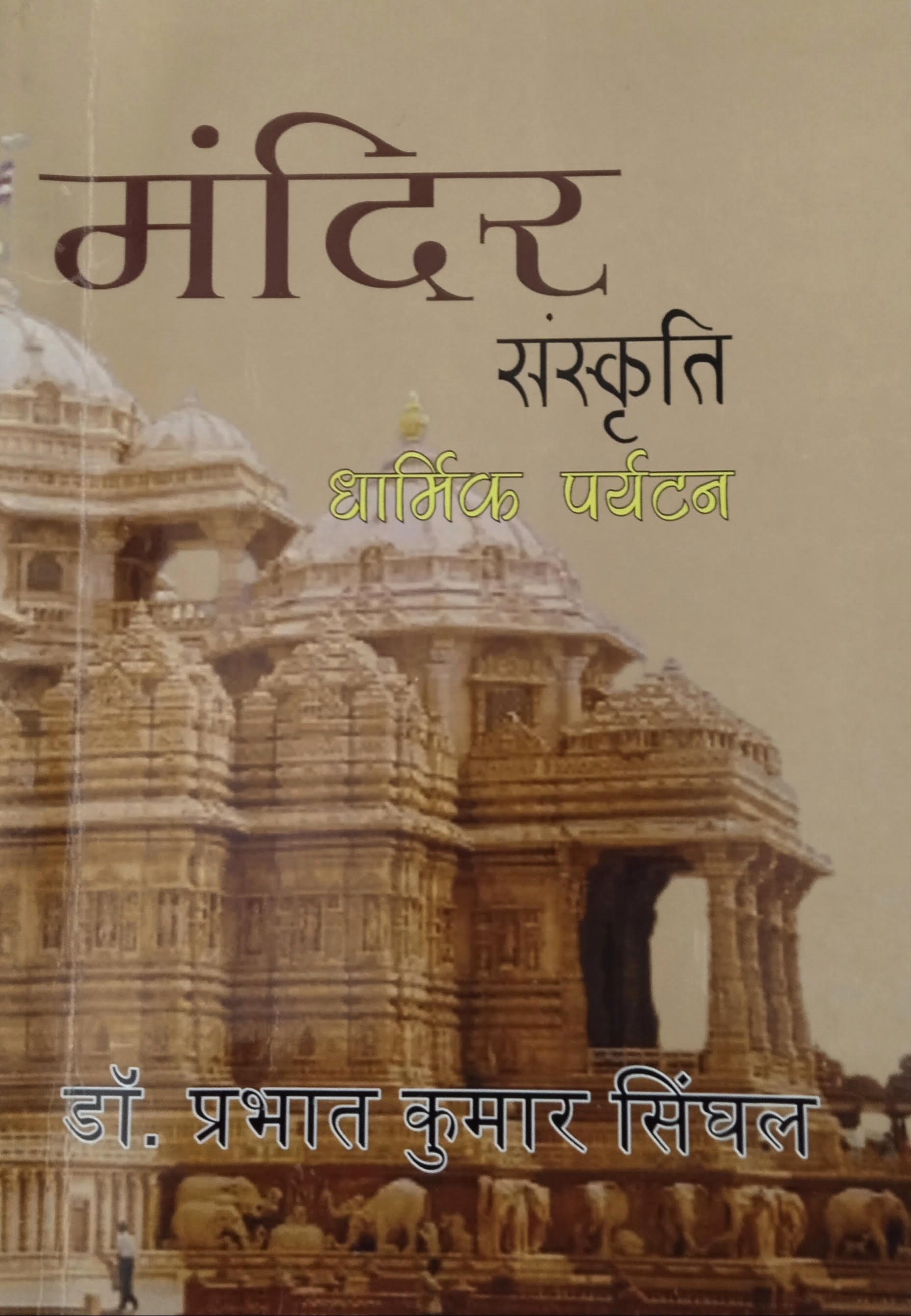
मंदिर वह पवित्र स्थान है, जहाँ देवताओं का वास है, एक दिव्यानुभूति का आभास है। जहाँ " मन का द्वार" प्रभु चरणों में समर्पित हो खुल जाता है। भारतीय संस्कृति व परम्परा में मंदिर उपासना, आराधना, तपस्या व त्याग का स्थल है, जहाँ मनुष्य अपने दंभ को त्याग कर पूर्णतः आस्था और विश्वास के साथ ईश्वर में लीन होकर सभी दुख प्रभू के समक्ष प्रकट कर देता है , स्वयं चिंता मुक्त होकर निश्चिन्त हो जाता है।
आत्मा परमात्मा में लीन होकर दिव्यता की अनुभूति करती है। यही भारतीय संस्कृति का प्रबल धार्मिक व आध्यात्मिक पक्ष है। मंदिर ऐसी धार्मिक आस्था का केंद्र है जहाँ मानवता की समृद्धि व " वसुधैव कुटुबंकम्" की भावना स्वत: ही जाग्रत होती है, जहाँ समस्त दुर्भावनाओं को मानव तिलांजलि दे , ईश्वर की शरण में चला जाता है ,इसलिए देवस्थान ऐसी सामाजिक व सांस्कृतिक एकता का केंद्र है जहाँ धार्मिक व आध्यात्मिक उन्नयन की दिव्य अनुभूति स्वत: ही जाग्रत होती है।
मंदिर में दीप प्रज्ज्वलन मंत्रोच्चारण ,अभिषेक, पूजा, पाठ, सेवा व घंटी का निनाद एक आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है,
इससे ईश्वर के आभास का अनुभव होता है और मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, नई आशा का संचार होता है।
मंदिर भजनों और शास्त्रीय नृत्यों से हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। दक्षिण भारत में कई मंदिर शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध हैं। हवेली संगीत जो मंदिर संगीत भी कहा जाता है, भारत की एक प्राचीन संगीत परंपरा है जो मंदिरों, विशेषकर वैष्णव मंदिरों, में गाए जाने वाले भजनों और कीर्तनों पर आधारित है। यह भक्ति संगीत का एक रूप है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है और राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथजी मंदिर जैसे मंदिरों में प्रमुखता से गाया जाता है। हवेली संगीत में विभिन्न रागों और तालों का उपयोग किया जाता है, जो दिन के समय और ऋतु के अनुसार बदलते रहते हैं। हवेली संगीत में अष्टयाम सेवा का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जो दिन के आठ पहरों में भगवान की लीलाओं का चित्रण करती है। यह संगीत भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना को व्यक्त करता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। यह कलात्मक अभिव्यक्ति है जो संगीत, भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव को जोड़ती है।
मंदिर संस्कृति की ऐसी ही विशेषताओं के आधार पर आधारित है कला, संस्कृति और पर्यटन लेखक डॉ.प्रभात कुमार सिंघल की " मंदिर संस्कृति - धार्मिक पर्यटन" पुस्तक। विशेषता यह है कि यह पुस्तक पाठक को जहां मंदिरों के क्रमिक विकास से अवगत करवाती है वहीं विभिन्न श्रेणियों में मंदिरों की यात्रा करवाती है और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक है।
पर्यटन की दृष्टि से मंदिरों के महत्व पर चर्चा करें तो भारत में जिस तेजी से धार्मिक श्रेत्र में पर्यटन का विकास हुआ है वह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पिछले दिनों में अयोध्या, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन में महाकाल, जम्मू स्थित वैष्णो देवी मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं यमनोत्री , दिल्ली में अक्षरधाम, जैसे कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ धार्मिक पर्यटन को पुष्ट करती है। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या धार्मिक पर्यटन का हब बन कर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन केंद्र बन गया है। विभिन्न मंदिरों सहित, बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं सिक्ख धर्म के कई पूजा स्थलों को जोड़ते हुए धार्मिक पर्यटन सर्किटों का विकास कर मूलभूत सुविधाएं विकसित हुई है। कई मंदिरों के कॉरिडोर बनने से पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आज पर्यटन का दायरा ताजमहल, गोवा, कश्मीर ,शिमला जैसे पर्यटक स्थलों से बाहर निकल कर धार्मिक पर्यटन की दिशा में तेजी से आगे आया है। योग एवं आयुर्वेद को भी वैश्विक ख्याति प्राप्त हुई है।
प्रस्तुत पुस्तक में मंदिरों की जानकारी पाठक को देने के लिए आठ अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय आदिकाल से वर्तमान समय तक मंदिरों के क्रमिक विकास , निर्माण और कला शैलियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। दूसरे अध्याय में भारत के मुख्य चार धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ पूरी, द्वारिका सहित हिमालय के लघु चार धाम की यात्रा का वर्णन है। तीसरा अध्याय प्राचीन काल से प्रचलित धार्मिक सप्तपुरियों अयोध्या, मथुरा, द्वारका, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम की यात्रा पर केंदित है। चौथा अध्याय हिंदुओं की देवी दुर्गा के आस्था के धाम 51 शक्तिपीठ के दर्शन करवाता है। पांचवां अध्याय शिव पुराण में वर्णित द्वादश ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, नागेश्वर, सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, घृष्णेश्वर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, पर आधारित है।
यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भारत के विरासत मंदिर छटे अध्याय की शोभा बने हैं। इनमें बिहार का महाबोधि मंदिर, मध्यप्रदेश का खजुराहो एवं सांची के स्तूप, ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, कर्नाटक का हम्पी और पत्तदकल मंदिर, तेलंगाना का काकातिया ( रामापपा ) रुद्रेश्वरा मंदिर, तमिलनाडु का महाबलीपुरम , ऐरातेश्वर, बृहदेश्वर एवं
गांगेयकोंडा चोलेश्वर मंदिर शामिल हैं।
अध्याय सात में उत्तर भारत के प्रमुख मंदिर
जम्मू कश्मीर ने मां वैष्णव देवी, अमरनाथ, पंजाब में स्वर्ण मंदिर, वृंदावन में बांके बिहारी, इस्कॉन, दिल्ली में स्वामी नारायण अक्षरधाम, महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक, शिरडी, शनि शिंगणापुर, राजस्थान में गोविंददेव, सांवलिया सेठ, ब्रह्मा मंदिर, श्रीनाथ जी, देलवाड़ा, रणकपुर, जगदीश मंदिर, इकलिंग जी, सालासर बाला जी, खाटूश्याम जी, पालीताणा, श्री सम्मेद शिखर, ओडिशा मैं लिंगराज, मुक्तेश्वर, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर, दक्षिणेश्वर काली और बेलूर मठ की यात्रा शामिल है। आठवां और अंतिम अध्याय दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों पर केंद्रित है। आंध्रप्रदेश में तिरुपति बाला जी,मैसूर में श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में होयसलेश्वर, तमिलनाडु में मीनाक्षी, केरल में श्री रंगास्वामी, कन्याकुमारी एवं गुरुवर मंदिर शामिल हैं।
पुस्तक की भूमिका में मध्य पश्चिम रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर अनुज कुमार कुच्छल लिखते है," मन्दिर में पत्थर से बनी मूर्ति निर्जीव नहीं है वरन् सजीव प्रतिमा है, इसका एहसास बनाए रखने के लिए मन्दिर में स्थापित करने से पूर्व विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कराई जाने का अनिवार्य नियम बनाया गया। मन्दिर की अपनी आचार संहिता बनाई गई। सजीव मान कर प्रतिमा को भोग लगाने, ऋतुओं के आधार पर वस्त्र धारण कराने, सुबह शाम आरती करने, दैनिक दिनचर्या शुरू करने से पूर्व स्नान कर शुद्ध होकर दर्शन के लिए मन्दिर जाने आदि के नियम बनाए गए। सदाचार और ज्ञान के प्रसार के लिए मंदिरों में सत्संग, कीर्तन, संतों के प्रवचन एवं अन्य धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के कार्यक्रम आयोजित करने के प्रावधान किए गए। यह पुस्तक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगी।"
अपने लेखकीय में लेखक लिखते हैं, "मन्दिर केवल धर्म से ही नहीं वरन समाज से जुड़े सम्पूर्ण संस्कृति का महान द्योतक हैं। प्राचीन शास्त्रों में निर्धारित वास्तु नियमानुसार मंदिरों का निर्माण किया जाता रहा हैं, जिससे मंदिर में आने वाले को सकारात्मक ऊर्जा और मन को शांति मिलती है। धर्म एवं आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ मंदिरों का, शिल्पियों को रोजगार देने, संगीत, नृत्य, ललित कलाओं का संरक्षण करने, चढावे से शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने, संतों के धार्मिक प्रवचनों से ज्ञान का प्रसार एवं अन्न भंडारों से पशुओं को चारा और भूखों को भोजन कराने में महत्व पूर्ण योगदान रहा हैं। हाल ही में विश्व व्यापी कोरोना बीमारी में भारत के मंदिरों का खजाना देश की मदद में काम आया। संस्कृति संरक्षण में सहायक हमारे प्राचीन और अधुनातन मन्दिर भारत में पर्यटन विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। श्रद्धालु जब किसी मन्दिर के दर्शनार्थ यात्रा करते हैं तो समीप के अन्य दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण करते हैं।"
साभार :
© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.






